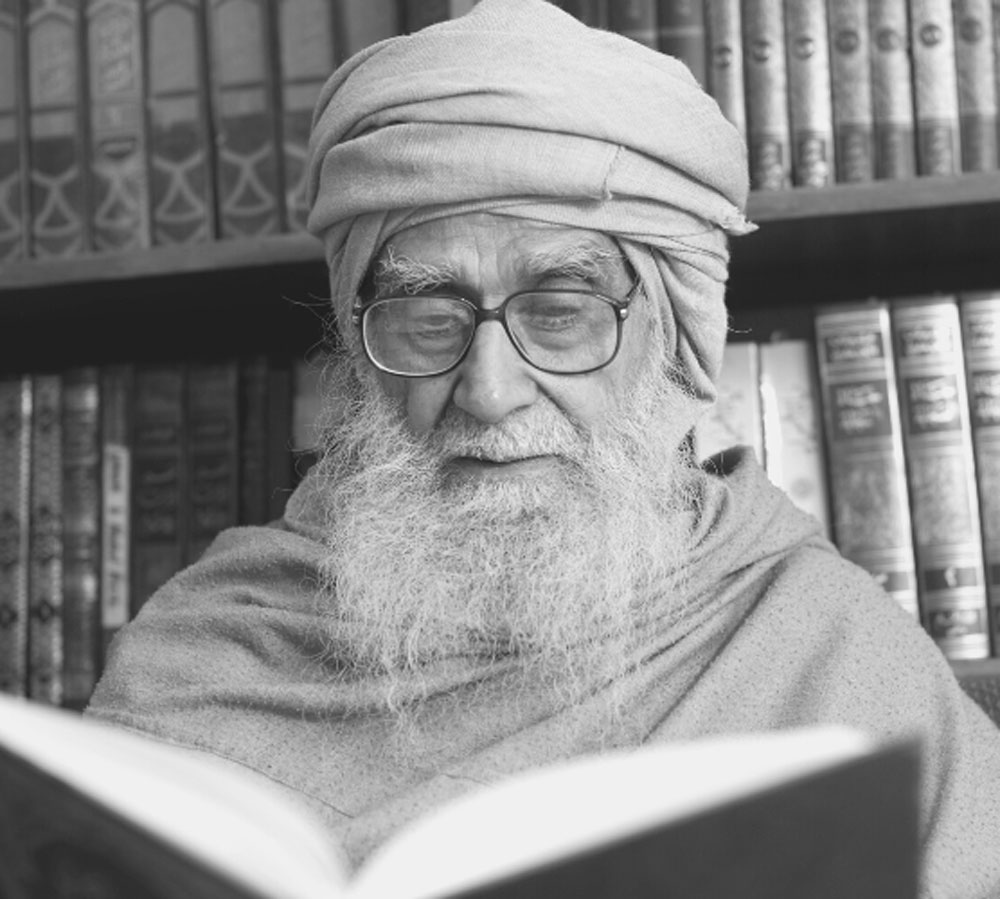पैग़ंबर-ए-इस्लाम का एक संबोधन हदीस की विभिन्न किताबों में आया है। पैग़ंबर के साथी कहते हैं— “हज़रत मुहम्मद हमारे बीच खड़े हुए और अपने ज़माने से लेकर क़यामत तक पेश आने वाली सारी बातें आपने हमें बताईं। इस संबोधन में आपने अपने अनुयायियों को बहुत सख्त़ी के साथ राजनीतिक बग़ावत से मना किया। आपने कहा कि कोई शासक चाहे तुम्हारे लिए ज़ालिम हो, वह तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे और तुम्हारा माल छीन ले, तब भी तुम उसकी आज्ञा का पालन करो।
इसके बाद आपने कहा कि मैं अपने अनुयायियों के लिए सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाले लीडरों से डरता हूँ और जब मेरे मानने वालों में तलवार दाख़िल हो जाएगी तो वह इससे क़यामत तक हटाई न जाएगी। (सुनन अबू दाउद, हदीस नं० 4,252)
इस प्रकार की दूसरी हदीसों की रोशनी में इस हदीस पर ग़ौर किया जाए तो इसका मतलब यह समझ में आता है कि राजनीतिक मामलों में पैग़ंबर-ए-इस्लाम ने सख़्ती के साथ हिंसात्मक काम से रोका और शांतिपूर्ण काम की नसीहत की। इसलिए कि हिंसक काम की परंपरा अगर एक बार क़ायम हो जाए तो इसके बाद उसे समाप्त करना बेहद कठिन हो जाता है।
किताबों में ज़्यादातर इस प्रकार की हदीसें आई हैं जिनमें आपने शासक के ख़िलाफ़ विद्रोह करने को अंतिम सीमा तक मना किया है।
इस आधार पर इस्लामी विद्वानों ने इस पर सहमति कर ली है कि स्थापित राज्य के ख़िलाफ़ किसी भी कारणवश विद्रोह करना हराम (अवैध) है। (अल ग़ुलू फ़िद्दीन, पृष्ठ संख्या 417)
एक ओर शासक के ख़िलाफ़ हिंसात्मक राजनीतिक गतिविधियाँ निषेध हैं और दूसरी ओर वर्णनों में आया है कि पैग़ंबर-ए-इस्लाम ने फ़रमाया— “श्रेष्ठ जिहाद यह है कि कोई व्यक्ति अत्याचारी राजा के सामने सच बात कहे।” (मुसनद अहमद, हदीस नं०11,143)
इन दोनों हदीसों पर ग़ौर करने से मालूम होता है कि किसी को कोई शासक अत्याचारी दिखाई दे, तब भी इसके लिए ज़्यादा-से-ज़्यादा जिस हद तक जाने की अनुमति है, वह केवल बातचीत द्वारा सुझाव (advice) देना है, न कि व्यवहारतः विरोधपूर्ण राजनीति करना या शासक को हटाने की कोशिश करना। दूसरे शब्दों में यह कि इस्लाम में केवल शांतिपूर्ण संघर्ष (peaceful struggle) है। हिंसापूर्ण संघर्ष (violent struggle) किसी भी हाल में और किसी भी कारणवश इस्लाम में जायज़ नहीं।
इस्लाम के बाद के इतिहास की संभवतः सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि कथित स्पष्ट आदेशों के बावजूद बाद की मुस्लिम पीढ़ियों में जिहाद के नाम पर हिंसात्मक राजनीति की परंपरा चल पड़ी, यहाँ तक कि यह मानसिकता मुसलमानों पर इतनी छा गई कि ‘दीन-ए-रहमत’ (क़ुरआन, 21:107) इनके यहाँ जंग का दीन बन गया। बाद की शताब्दियों में तैयार होने वाला ज़्यादातर साहित्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी मानसिकता और विचारधारा को दर्शाता है।
बाद के ज़माने में क़ुरआन की जो व्याख्याएँ लिखी गईं, उनमें इस मानसिकता को दर्शाया गया, जैसे कि क़ुरआन की इन व्याख्याओं में कहा गया कि जंग का आदेश उतरने के बाद धैर्य व उपेक्षा की आयतें निरस्त हो गईं। हदीसों को एकत्र करके संकलित किया गया तो उनमें जो हदीसें जिहाद को लेकर थीं, उन्हें हदीस की किताबों में बहुत विस्तार के साथ जिहाद के अध्याय में एकत्र किया गया, मगर दावत यानी सच्चाई से अवगत कराने का अध्याय किसी भी पुस्तक में शामिल नहीं। यही हाल इस्लामी धर्मशास्त्र की समस्त पुस्तकों का है। धर्मशास्त्र की पुस्तकों में जिहाद और जिहाद से संबंधित आदेश बड़े विस्तार के साथ बताए गए हैं, मगर दावत का अध्याय किसी भी धर्मशास्त्र की पुस्तक में नहीं।
यही हाल बाद में लिखे जाने वाले लगभग समस्त इस्लामी साहित्य का हुआ। प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान इब्ने तैमिया से लेकर शाह वली उल्लाह तक और शाह वली उल्लाह से लेकर मौजूदा ज़माने के विद्वानों तक, कोई भी व्यक्ति दावत व तबलीग़ (प्रचार-कार्य)के विषय पर कोई पुस्तक तैयार न कर सका। अगर किसी किताब का नाम दावत व तबलीग़ है तो भी उसमें राजनीति की बातें हैं या धार्मिक क्रिया की श्रेष्ठता की बातें हैं। उसमें दावत व तबलीग़ की कोई बात नहीं।
इस प्रकार के साहित्य से मुसलमानों का जो स्वभाव बना, उसी का यह परिणाम है कि मुसलमानों में टकराव का तरीक़ा अपनाने वाले लोग हीरो बन जाते हैं और जो व्यक्ति अमन का तरीक़ा अपनाए, वह उनमें अलोकप्रिय होकर रह जाता है।
इसी कारण ऐसा हुआ कि इमाम हुसैन के चरित्र को तो हमारे वक्ताओं और लेखकों ने ख़ूब व्यक्त किया, मगर इमाम हसन का चरित्र व्यक्त न किया जा सका। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुस्लिम विजेता को मुसलमानों के बीच ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई, मगर वह लोग जिन्होंने तातारी आक्रमणकारियों को इस्लाम का संदेश पहुँचाकर उन्हें इस्लाम का सेवक बनाया, उनकी कोई चर्चा हमारी इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलती। वर्तमान समय में उसामा बिन लादेन जैसे हिंसा की बात करने वाले लोग बड़ी सरलता से मुसलमानों के बीच हीरो बन जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति शांति और मानव सम्मान की बात करे तो वह मुसलमानों के बीच सार्वजनिक लोकप्रियता हासिल न कर सकेगा।
इस सोच की सबसे बड़ी हानि यह है कि इंसानियत मुसलमानों का कंसर्न (concern) ही न रही। मुसलमानों का हाल यह हुआ कि ईश्वर के बंदों को वे अपनी क़ौम और ग़ैर-क़ौम (we and they) में बाँटकर देखने लगे। दावती विचारधारा के अनुसार, मुसलमान और ग़ैर-मुसलमान का रिश्ता दाई (परीचय देने वाला) और मदऊ (जिसको परिचित कराया जाए) का है। इसके विपरीत जिहादी (जंग के मतलब में) विचारधारा में यह होता है कि मुसलमान दूसरों को अपना प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन समझने लगते हैं।
पश्चिमी समुदाय के वर्चस्व के बाद यह अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुसलमानों को प्रतीत हुआ कि पश्चिमी समुदायों ने उनसे उनकी श्रेष्ठता का स्थान छीन लिया है। इसके नतीजे में यह हुआ कि प्रतिद्वंद्विता और ज़्यादा वृद्धि के साथ नफ़रत बन गई। मुसलमान आम तौर पर दूसरे समुदायों को दुश्मन की नज़र से देखने लगे।