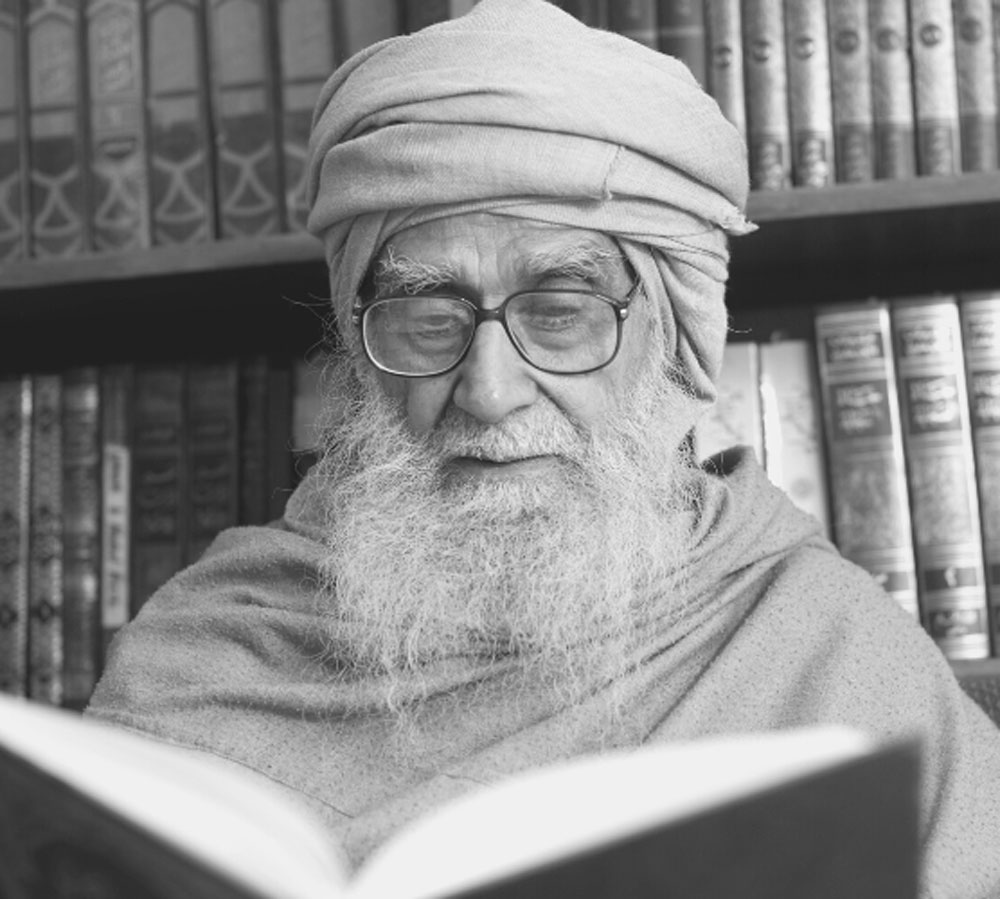सांप्रदायिक झगड़ों में अक्सर धर्म का नाम प्रयोग किया जाता है। बार-बार ऐसा होता है कि कोई राजनीतिक या क़ौमी चीज़ धार्मिक विवाद बन जाती है और तेज़ी से लोगों की भावनाएँ भड़क उठती हैं, जो भिन्न वर्गों के बीच हिसांत्मक टकराव का कारण बन जाती हैं। इसी कारण बहुत से लोग स्वयं धर्म के विरोधी बन गए हैं। उनका कहना है कि इंसान को धर्म की आवश्यकता नहीं, इसलिए धर्म का ख़ात्मा कर देना चाहिए। धर्म को समाप्त करे बिना सामाजिक एकता संभव नहीं, मगर यह एक अतिवाद के उत्तर में दूसरा अतिवाद है। यह धार्मिक अतिवादिता का मुक़ाबला धर्मनिरपेक्ष अतिवादिता से करना है, जो न तो संभव है और न फ़ायदेमंद। असल यह है कि धर्म अपने आपमें स्वयं कोई समस्या नहीं। धर्म इंसानी जीवन का एक स्वस्थ अंश है। जो चीज़ समस्या है, वह कुछ स्वार्थी लोगों की ओर से धर्म का राजनीतिक शोषण (exploitation) है। इसलिए असल काम शोषण को समाप्त करना है, न कि स्वयं धर्म को।
धर्म के दो भाग हैं— व्यक्तिगत और सामूहिक। धर्म के व्यक्तिगत भाग से तात्पर्य आस्था, उपासना, आचरण और आध्यात्मिकता है और सामूहिक भाग से अभिप्राय उसके राजनीतिक और सामाजिक आदेश है। इस मामले में सही तरीक़ा यह है कि सामान्य परिस्थितियों में केवल धर्म के व्यक्तिगत भाग पर बल दिया जाए। सारा ध्यान धर्म की रूह (spirit) को ज़िंदा करने पर लगाया जाए।
जहाँ तक धर्म के सामाजिक और राजनीतिक आदेशों का मामला है, उसे उस समय तक न छेड़ा जाए, जब तक पूरा समाज उसके लिए तैयार न हो। सामाजिक और राजनीतिक आदेश पूरे समाज की सामूहिक सहमति से स्थापित हो सकते हैं। इसलिए ऐसे आदेशों के मामले में किसी व्यावहारिक अग्रसरता से उस समय तक बचना चाहिए, जब तक पूरे समाज का सामूहिक इरादा उसके अनुकूल न हो जाए।
इस मामले को धर्म और राजनीति के बीच व्यावहारिक भेद कहा जा सकता है अर्थात सैद्धांतिक रूप से राजनीति को धर्म का हिस्सा मानना, लेकिन वास्तविकताओं के आधार पर राजनीतिक आदेशों को लागू करने को विलंबित या स्थगित कर दिया जाए। इसी का नाम नीति या समझदारी (wisdom) है। इस नीति का यह लाभ है कि धर्म और राजनीति दोनों की माँग पूरी हो जाती है। धर्म की माँग वर्तमान में और राजनीति की माँग भविष्य में। इसके विपरीत अगर इस नीति का लिहाज़ न रखा जाए और दोनों पक्षों को एक साथ उभार दिया जाए तो परिणाम यह होगा कि धार्मिक माँगें और राजनीतिक माँगें दोनों ही पूरी होने से रह जाएँगी।