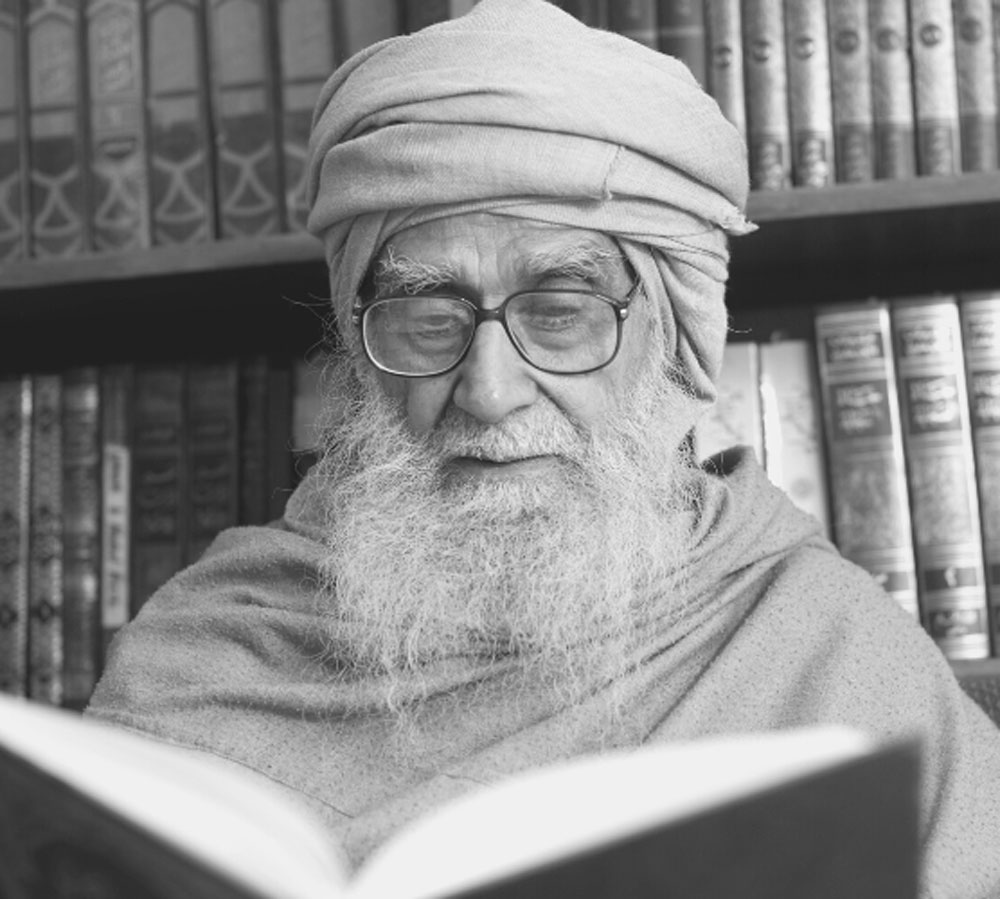चुप रहिए
क़ुरआन में है कि कान और आँख और दिल, हर चीज़ के बारे में इन्सान से पूछ होगी (बनी इस्राईल 36)। हदीस में आया है कि तुम में जो शख़्स फ़तवा देने में ज़्यादा जरी (दुस्साहसी) है वह जहन्नम के ऊपर ज़्यादा जरी है।
इसलिए फ़त्वा देने के मामले में सहाबी बेहद एहतियात बरतते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के बारे में हदीस में आया है कि अब्दुल्लाह तराज़ू में उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी हैं। इसके बावजूद उनका यह हाल था कि वह कूफ़ा में थे। उन से एक मामले में पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। लोग उनसे महीने भर पूछते रहे। यहां तक कहा कि अगर आप ही फ़त्वा न देंगे तो हम किस से पूछें? फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हमेशा फ़त्वा देने से परहेज़ करते थे। लोग जब ज़ोर डालते तो कहते कि हमारी पीठ को जहन्नम के लिए सवारी न बनाओ।
इन रिवायतों में फ़त्वे से मुराद कोई सीमित फ़त्वा नहीं है। इसका तअल्लुक़ उन तमाम बातों से है जो मुसलमानों के साथ होती हैं और जिनमें वे अपने आलिमों और अपने रहनुमाओं से राय पूछते हैं। ऐसे मामलों में आलिमों और रहनुमाओं का फ़र्ज़ है कि वे बोलने से ज़्यादा सोचें। वे उस वक़्त तक कोई बयान न दें जब तक इस मामले में मश्वरा, और ग़ौरो-फ़िक्र की तमाम शर्तों को आख़िरी हद तक पूरा न कर चुके हों। ऐसे मामलों में न बोलना इससे बेहतर है कि आदमी ग़ैरज़िम्मेदाराना तौर पर बोलने लगे।
सामूहिक मामलों में राय देना बेहद नाज़ुक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर राय ग़लत हो तो लोगों को नामालूम मुद्दत तक उसका नुक़सान भुगतना पड़ता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि अगर वह बोलना चाहता है तो पहले उसकी तमाम शर्तों को पूरा करे, उसके बाद अपनी राय ज़ाहिर करे।