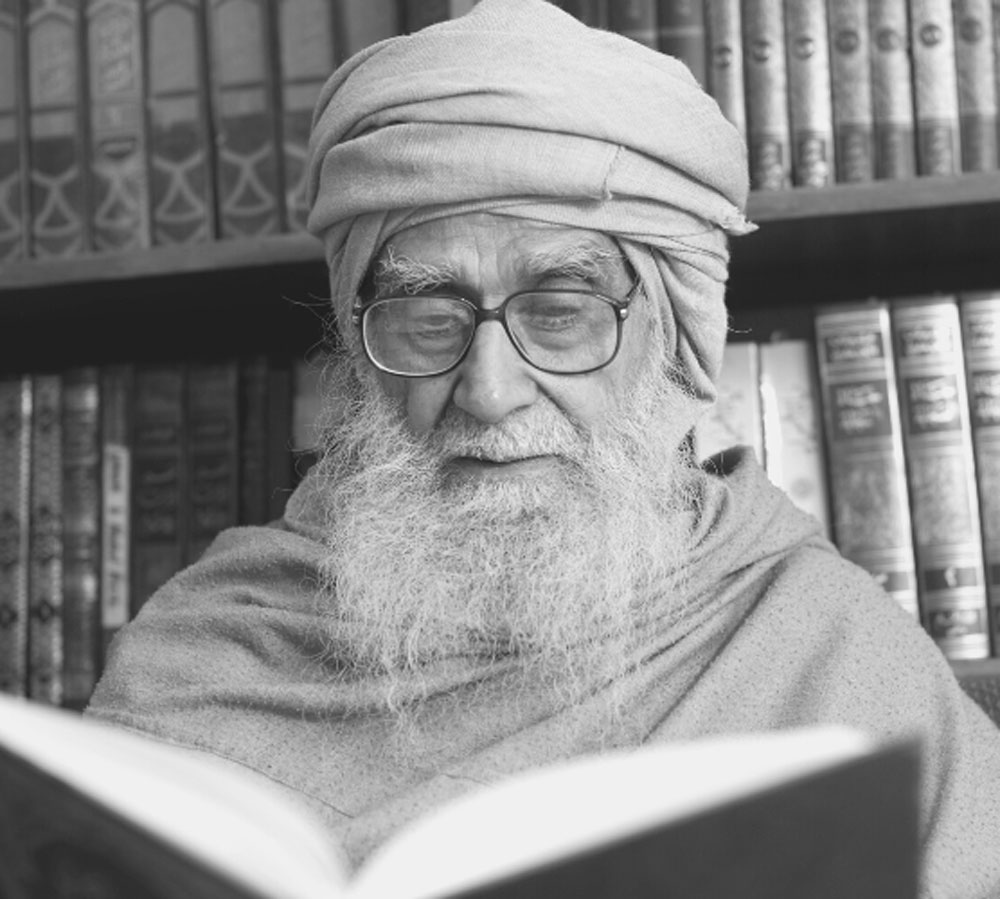पैग़ंबरे-इस्लाम के तरीक़े का एक पहलू यह था कि आपकी नज़र हमेशा हक़ाइक़ (spirit) पर रहती थी, न कि ज़ाहिर सूरत पर। ज़वाहिर में अगर बेख़बरी की बिना पर कोई फ़र्क़ हो जाए तो उसे नाक़ाबिल लिहाज़ समझते थे। अलबत्ता हक़ीक़ी अहमियत वाली बातों के बारे में आपका रवैया हमेशा बहुत सख़्त होता था।
पैग़ंबरे-इस्लाम के आख़िरी हज का एक वाक़या अल-बुख़ारी, मुस्लिम और अबू-दाऊद में थोड़े-थोड़े लफ़्ज़ी फ़र्क़ के साथ आया है। यह आपकी ज़िंदगी का आख़िरी साल था। आप हज के फ़राइज़ अदा करने के बाद मीना में बैठे हुए थे। लोग आपके पास आते और हज के मसाइल दरयाफ़्त करते। कोई कहता कि मुझे मसला मालूम न था, चुनाँचे मैंने ज़िबह करने से पहले बाल मुँड़वा लिए। कोई कहता कि मैंने रमी से पहले क़ुर्बानी कर ली वग़ैरह-वग़ैरह।
आप हर एक से कहते कि कर लो, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह बार-बार लोग आते रहे और आगे-पीछे की बाबत सवाल करते रहे। आप हर एक से यही कहते कि कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं— ला हर्जा, ला हर्जा (मसनद अहमद, हदीस नंबर 1857)।
अबू दाऊद की रिवायत नंबर 2015 में इन अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा है— कर लो कोई हर्ज नहीं। हर्ज तो उस शख़्स के लिए है, जो एक मुसलमान को बेइज़्ज़त करे। ऐसा ही शख़्स ज़ालिम है। यही वह शख़्स है, जिसने हर्ज किया और हलाक़ हुआ।
दीन में असल अहमियत मायने की है, न कि ज़वाहिर की। एक शख़्स ज़ाहिरी चीज़ों का ज़बरदस्त एहतमाम करे, लेकिन मअनवी पहलू के मामले में वह ग़ाफ़िल हो तो ऐसा शख़्स इस्लाम की नज़र में बेक़ीमत हो जाएगा। अल्लाह हमेशा आदमी की नियत को देखता है। नियत अगर अच्छी है तो ज़ाहिरी चीज़ों में कमी या फ़र्क़ को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, लेकिन अगर आदमी की नियत अच्छी न हो तो अल्लाह की नज़र में उसकी कोई क़ीमत नहीं, चाहे उसने ज़वाहिर के मामले में कितना ही ज़्यादा एहतमाम कर रखा हो। ज़ाहिरी ख़ुशनुमाई से इंसान फ़रेब में आ सकता है, लेकिन ज़ाहिरी खुशनुमाई की ख़ुदा के नज़दीक कोई क़ीमत नहीं।