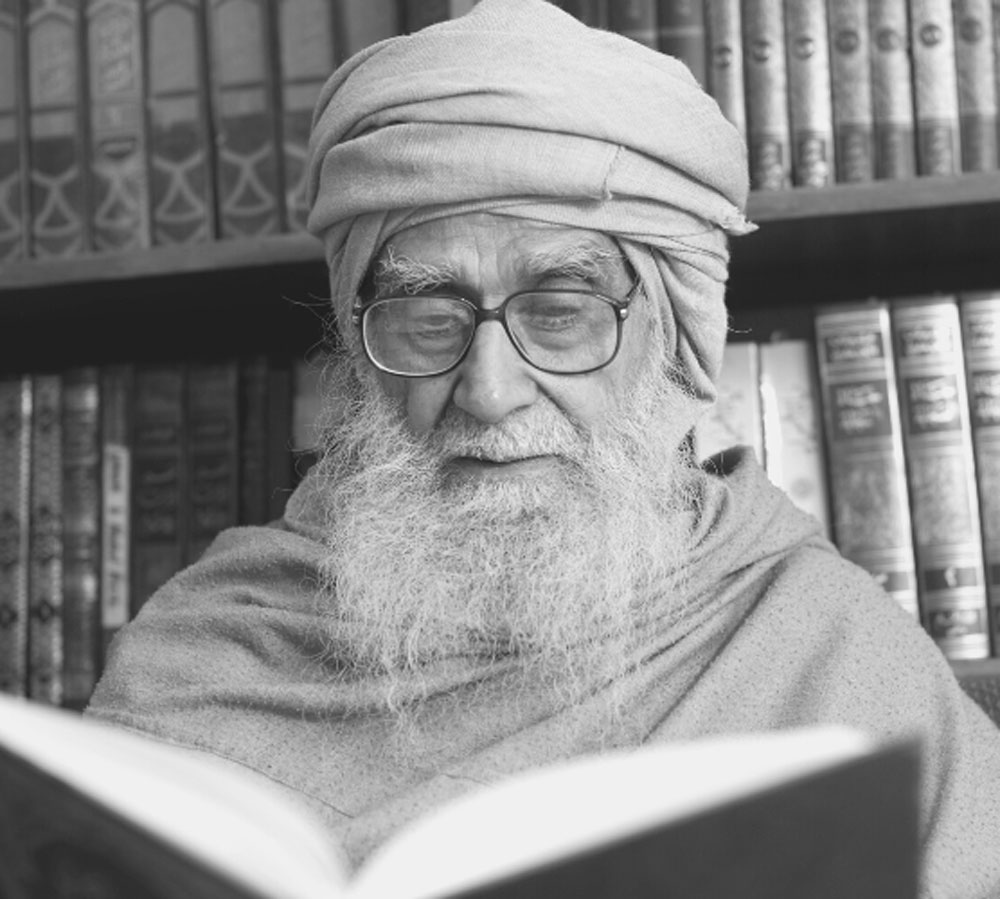सवाल
आपको लफ़्ज़-ए-जिहाद की तारीफ़ में कुछ लीफ़लेट्स रवाना किए जा रहे हैं। ग़ौर और सब्र के साथ पढ़कर उनका जवाब दें। उन्हें पढ़कर यही समझ में आता है कि क़ुरआन को ख़ुदाई किताब कहने वाला इंसानियत का दुश्मन है और सर्वधर्म समभाव का भी दुश्मन है। (शिव गौड़, संगारेड्डी)
जवाब
शिव गौड़ साहिब ने अपने इस ख़त के साथ हमें अंग्रेज़ी में 41 सफ़हात की फ़ोटो कॉपियाँ भेजी हैं। इसका जवाब यहाँ तहरीर किया जाता है। आपने अपने ख़त में 24 आयतें नक़ल की हैं, जिनमें इस तरह की बातें हैं कि उनसे लड़ो, उनसे दोस्ती न करो, उनके साथ नरमी से न पेश आओ। उनके ख़िलाफ़ जिहाद करो वग़ैरह-वग़ैरह।
वाज़ेह रहे कि क़ुरआन की ये आयतें जो आपने नक़ल की हैं, वे ग़ैर-मुसलमान के साथ मुसलमान के ताल्लुक़ को नहीं बतातीं, बल्कि वे जंग करने वालों के साथ मुसलमान के ताल्लुक़ को बताती हैं और जंग के मुआमले में यही सारी दुनिया का माना हुआ (accepted) उसूल है। इन आयतों की बुनियाद पर आपने इस्लाम के बारे में जो शदीद राय क़ायम की है, वह सरासर ग़लतफ़हमी पर मबनी है। आपने क़ुरआन की मज़्कूरा आयतों को आम मायनों में ले लिया है। हालाँकि ये आयतें हंगामी हालात के लिए हैं। ये उस वक़्त के लिए हैं, जबकि मुसलमानों और दूसरी क़ौम के दरम्यान जंग (state of war) क़ायम हो गई हो और यह एक मालूम हक़ीक़त है कि हालत-ए-जंग में हमेशा ऐसा ही किया जाता है। जहाँ तक नॉर्मल हालात में लोगों के साथ मुसलमान के सुलूक का ताल्लुक़ है, वह दूसरी आयतों से मालूम होता है, जो क़ुरआन में कसरत से मौजूद हैं।
इन दूसरी आयतों में मुसलमानों को तमाम इंसानों के साथ हमदर्दी और ग़मख़ारी का सुलूक करने का हुक्म दिया गया है (सूरह अल-बलद, 90:17)। इसी तरह हुक्म है कि दरगुज़र (tolerance) का तरीक़ा इख़्तियार करो। (सूरह अल-आराफ़, 7:199)
इसी तरह पैग़ंबर-ए-इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया— “उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह अपनी रहमत सिर्फ़ रहम करने वाले पर करता है।” (मुसनद अबू यअला, हदीस नं० 4,258)। लोगों ने कहा हम सब रहम करते हैं, आपने कहा कि तुम्हारा अपने साथी पर रहम करना मुराद नहीं है, तमाम इंसानों के साथ रहम का मुआमला किया जाए वग़ैरह-वग़ैरह ।
जिन लोगों ने तुमसे जंग नहीं की, तुम्हें भलाई का मुआमला करना चाहिए, मगर जो लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके साथ बतौर डिफेंस जंग करो।
जहाँ तक ग़ैर-मुसलमानों से ताल्लुक़ का मुआमला है, क़ुरआन में उसकी बाबत एक बुनियादी उसूल मुक़र्रर कर दिया गया है— “अल्लाह तुम्हें उन लोगों से नहीं रोकता, जिन्होंने दीन के मुआमले में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, तुम उनसे भलाई करो और तुम उनके साथ इंसाफ़ करो। बेशक अल्लाह इंसाफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह बस उन लोगों से तुम्हें मना करता है, जो दीन के मुआमले में तुमसे लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकलने में मदद की, तुम उनसे दोस्ती न करो और जो उनसे दोस्ती करे तो वही लोग ज़ालिम हैं।” (60:8-9)
क़ुरआन की इन दोनों आयात का मतलब यह है कि जिन लोगों ने तुमसे जंग नहीं की, तुम्हें भलाई का मुआमला करना चाहिए, मगर जो लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके साथ बतौर डिफेंस जंग करो। क़ुरआन के मुताबिक़, आम इंसानों को तकलीफ़ देना सख़्त मना है, दुश्मन (enemy) और लड़ने वाले (combatant) के दरम्यान भी फ़र्क़ करना चाहिए। क़ुरआन का हुक्म यह है कि बज़ाहिर अगर कोई शख़्स या गिरोह तुम्हारा दुश्मन हो, तब भी तुम्हें उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ क़ायम रखना चाहिए।
जैसा कि क़ुरआन में दूसरे मुक़ाम पर यह हुक्म दिया गया है कि एक शख़्स अगर बज़ाहिर तुम्हारा दुश्मन हो, तब भी तुम उसके साथ सबसे अच्छे तरीक़े पर मुआमला करो, ऐन मुमकिन है कि वह किसी दिन तुम्हारा दोस्त बन जाए। क़ुरआन में आया है—
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
“भलाई और बुराई दोनों बराबर नहीं। तुम जवाब में वह कहो, जो उससे बेहतर हो, फिर तुम देखोगे कि तुममें और जिसमें दुश्मनी थी, वह ऐसा हो गया, जैसे कोई दोस्त क़राबत वाला।” (41:34)
इन आयात से मालूम होता है कि अहल-ए-ईमान को जंग की इजाज़त सिर्फ़ उस वक़्त है, जबकि फ़रीक़-ए-मुख़ालिफ़ (opponent) की तरफ़ से हमले का आग़ाज़ हो चुका हो, लेकिन जो इस जंग में शामिल नहीं हैं, उन्हें बिलकुल भी तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, ख़्वाह वह दिल में दुश्मनी रखता हो। इंटरनेशनल मुआमलात में यही सारी दुनिया का माना हुआ उसूल है और इस्लामी शरीयत में भी इसी उसूल को इख़्तियार किया गया है।
वाज़ेह रहे कि क़ुरआन एक साथ एक वाहिद किताब की सूरत में नहीं उतरा, बल्कि वह हालात के ऐतबार से 23 साल के दौरान उतरा। 23 साल की इस मुद्दत को उमूमी तौर पर दो हिस्सों में तक़्सीम किया जा सकता है— एक 20 साल और दूसरा 3 साल। इस 23 साला मुद्दत के नुज़ूल में 20 साल गोया अमन के साल थे और तक़रीबन 3 साल जंगी हालात के साल। आपने जिन 24 आयतों का हवाला दिया है, वे मज़्कूरा तक़्सीम के मुताबिक़ 3 साल वाले इमरजेंसी के हालात में उतरीं। क़ुरआन की दूसरी आयतें जो 20 साल वाली मुद्दत में उतरीं, वे सब-की-सब अमन और इंसाफ़ और इंसानियत जैसी मुस्बत तालीमात पर मुश्तमिल (based) हैं।
सवाल
क़ुरआन में कई आयतें ऐसी हैं, जो मुसलमानों से कहती हैं कि काफ़िरों को क़त्ल करो। यही वजह है कि मुसलमान जिहादी हो गए हैं और ग़ैर-मुसलमानों को क़त्ल करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। मसलन क़ुरआन में यह आयत है—
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
“क़त्ल करो उन्हें, जिस जगह पाओ और निकाल दो उन्हें, जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला है। फ़ित्ना सख़्ततर है क़त्ल से और उनसे मस्जिद-ए-हराम के पास न लड़ो, जब तक कि वे तुमसे जंग न छेड़ें। पस अगर वे तुमसे जंग छेड़ें तो उन्हें क़त्ल करो। यही सज़ा है काफ़िरों की।” (2:191)
सवाल यह है कि क़ुरआन में जब तक इस तरह की आयतें मौजूद हैं तो मुसलमानों का ग़ैर-मुसलमानों के साथ शांति से रहना कैसे मुमकिन है। (अशोक सिंघल, दिल्ली)
जवाब
यह आयत ख़ुद ही यह बता रही है कि जंग का हुक्म काफ़िर के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि मुक़ातिल (हमलावर) के ख़िलाफ़ है। जैसा कि ख़ुद उसी आयत में कहा गया है— “पस अगर वे जंग छेड़ दें तो तुम भी दिफ़ा में उनसे जंग करो।”
इसी तरह मज़्कूरा आयत से पहले ये अल्फ़ाज़ हैं—
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
“जो लोग तुमसे जंग करते हैं, उनसे तुम (in self-defence) जंग करो और तुम ख़ुद जारहीयत (aggression) न करो।” (2:190)
चुनाँचे क़ुरआन और पैग़ंबर-ए-इस्लाम की सुन्नत का मुताला किया जाए तो यह मालूम होता है कि इस्लाम में सिर्फ़ दिफ़ाई जंग जायज़ है और इसका इख़्तियार भी सिर्फ़ हाकिम-ए-वक़्त को हासिल होता है, किसी ग़ैर-हुकूमती गिरोह को हथियारबंद जद्दोजहद (armed struggle) की हरगिज़ इजाज़त नहीं। इसी तरह इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में क़िताल का हुक्म एक वक़्ती (temporary) सबब के लिए है। वह इस्लाम का कोई ऐसा हुक्म नहीं है, जो हर लम्हा जारी रहे। जब दिफ़ा का सबब ख़त्म हो जाएगा तो जंग का हुक्म भी अमलन मौक़ूफ़ (suspend) हो जाएगा यानी जब अमन का ज़माना हो तो जंग नहीं की जाएगी। यही इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ में पेश आया। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में माज़ी के तसलसुल (continuation) के तहत जंग की सूरत पेश आई यानी उन्होंने पैग़ंबर-ए-इस्लाम के ख़िलाफ़ नाहक़ जंग छेड़ दी और इस तरह रसूलुल्लाह को दिफ़ाई (defensive) क़दम उठाने पर मजबूर कर दिया, मगर जंग का यह हुक्म वक़्ती था। क़ुरआन के अल्फ़ाज़ में जब फ़रीक़-ए-मुख़ालिफ़ ने अपना औज़ार (हथियार) रख दिया तो जंग का ख़ात्मा हो गया। (सूरह मुहम्मद, 47:4)
इस सिलसिले में दूसरी बात यह है कि क़ुरआन में जिन चंद मुक़ामात पर काफ़िर का लफ़्ज़ आया है, उससे पैग़ंबर-ए-इस्लाम के ज़माने के इनकार करने वाले मुराद हैं। कु़रआनी इस्तिलाह के मुताबिक़ ऐसा नहीं है कि लफ़्ज़ काफ़िर अबद तक के लिए हर ग़ैर-मुस्लिम गिरोह के लिए बोला जाएगा यानी काफ़िर किसी क़ौम या नस्ल का दाइमी (permanent) लक़ब नहीं है। चुनाँचे अहल-ए-इस्लाम ने बाद के ज़माने के लोगों के लिए जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए वे काफ़िर या कुफ़्फ़ार न थे, बल्कि ये वही अल्फ़ाज़ थे, जो कि कौमें ख़ुद अपने लिए इस्तेमाल कर रही थीं, मसलन हिंदू, यहूद, इसाई, पारसी, बौद्ध वग़ैरह। इस्लामी उसूल के मुताबिक़ किसी क़ौम को उसी नाम से पुकारा जाएगा, जो नाम जिसने ख़ुद अपने लिए इख़्तियार किया हो।
क़ुरआन के मुताबिक़ पैग़ंबरों ने जब अपने ज़माने के ग़ैर-मोमिन लोगों को पुकारा तो उन्होंने यह नहीं कहा कि ‘ऐ काफिरो’, बल्कि यह कहा कि ‘ऐ मेरी क़ौम के लोगो’। चुनाँचे क़ुरआन में पैग़ंबर की ज़बान से पचास बार ये अल्फ़ाज़ आए हैं— ‘या-क़ौमे’ (ऐ मेरी क़ौम) इसी तरह क़ुरआन में पैग़ंबरों के हम-ज़माना ग़ैर-मोमिनीन को उनकी क़ौम का नाम दिया गया है, मसलन क़ौम-ए-लूत, क़ौम-ए-सालेह, क़ौम-ए-हूद, क़ौम-ए-नूह वग़ैरह। हदीस में आया है कि पैग़ंबर को उनके मुख़ालिफ़ीन ने पत्थर मारा और उनकी पेशानी से ख़ून बहने लगा। उस वक़्त पैग़ंबर की ज़बान से निकला— “ऐ मेरे रब, मेरी क़ौम को माफ़ कर दे, क्योंकि वह लोग नहीं जानते।” (मुसनद अहमद, हदीस नं० 4,057)
इससे मालूम हुआ कि पैग़ंबरों का नज़रिया ‘दो क़ौमी नज़रिया’ (Two Nation Theory) न था, बल्कि वह ‘एक क़ौमी नज़रिया’ था यानी जो क़ौमियत पैग़ंबर की थी, वही क़ौमियत पैग़ंबर के मुख़ातबीन की भी थी। पैग़ंबर और उनके मुख़ातबीन के दरम्यान जो फ़र्क़ था, वह क़ौमियत का फ़र्क़ न था, बल्कि अक़ीदे और मज़हब का फ़र्क़ था। जैसा कि क़ुरआन में है—
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
“तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन।” (109:6)
क़ुरआन में अल-इंसान (वाहिद) का लफ़्ज़ 65 बार आया है और अल-नास (इंसान की जमा) 240 बार आया है। इसके मुक़ाबले में काफ़िर का लफ़्ज़ सिर्फ़ पाँच बार क़ुरआन में आया है और उसकी जमा अल-कुफ़्फ़ार, अल-काफ़िरून और अल-काफ़िरीन के अल्फ़ाज़ 150 बार आए हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि इस मुआमले में क़ुरआन का तसव्वुर क्या है। क़ुरआन की नज़र में यह ज़मीन दार-उल-इंसान (इंसान का घर) है, न कि दार-उल-हर्ब (जंग का मैदान)।